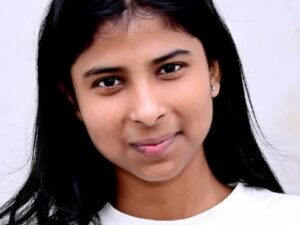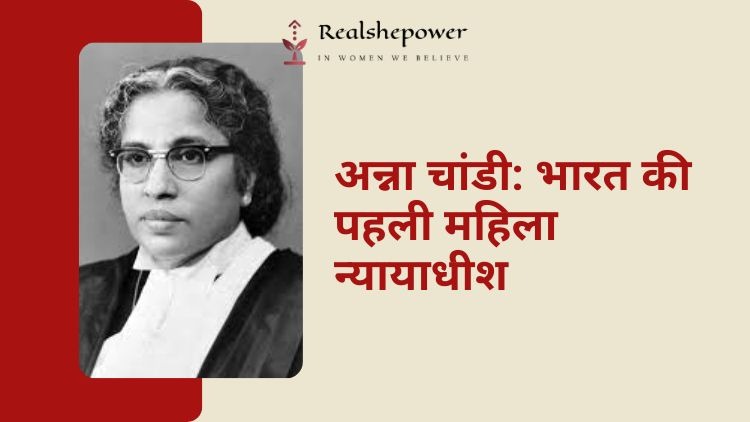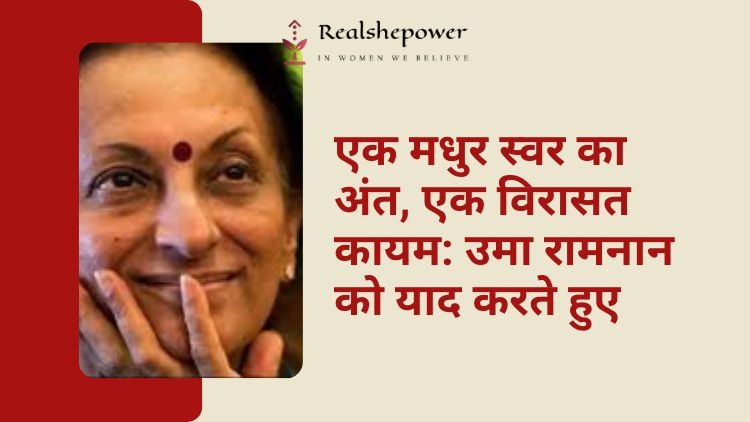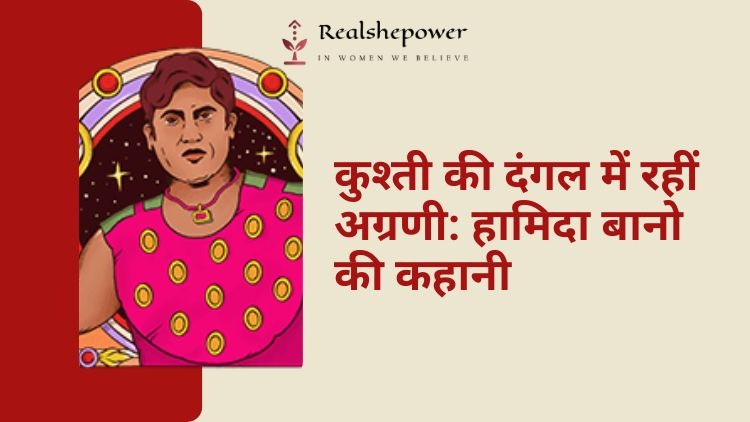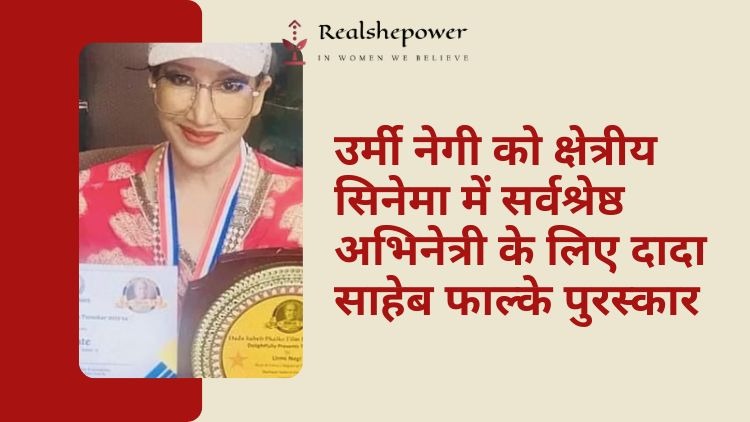गुलामी की सदियों में दुनिया के अनेक देशों ने अपने वस्त्र और अपनी संस्कृति
को बिसार दिया, पर भारत के कारीगर नहीं भूल पाए। अंग्रेजों ने कोशिश तो
बहुत की थी कि भारत अपनी प्रतिभा भूल जाए और केवल ‘गोरी-प्रतिभा’ का
ग्राहक बना रहे।
दुनिया अक्सर हम भारतीयों को कम आंकने की गलती करती है और हम भी अपने पारंपरिक वैभव की ओर से मुंह बिचकाने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि विदेशियों ने ही हमें सब कुछ सिखाया, हमें तो कुछ नहीं आता था। हमारे पास आखिर था ही क्या? पर सच यह है कि इस देश के बारे में आप क्या-क्या बताएंगे? यहां के कपड़ों की ही बात कर लीजिए। उनके रंगों में भी केवल सफेद की बात कर लीजिए, तो यहां श्वेत वस्त्रों के ही कम से कम 15 शेड्स हैं। श्वेत के इतने शेड्स किसी भी अन्य देश में नहीं हैं और अपना देश अकेला ऐसा है, जहां लाखों लोग आज भी बिना सिले कपड़े बहुत शौक से पहनते हैं।
गुलामी की सदियों में दुनिया के अनेक देशों ने अपने वस्त्र और अपनी संस्कृति को बिसार दिया, पर भारत के कारीगर नहीं भूल पाए। गोरों ने कोशिश तो बहुत की थी कि भारत अपनी प्रतिभा भूल जाए, केवल गोरी-प्रतिभा का ग्राहक बना रहे। यह कोशिश आज भी जारी है और भारतीय कारीगर खुद को दिलोजान से बचाने में जुटे हैं। 1960 के दशक के आखिर में भी कारीगर इसी कवायद में लगे थे। उनकी एक उजड़ती हुई बस्ती कोलकाता के बाहरी इलाके सेरामपुर हुआ करती थी। वहां के पुश्तैनी कारीगर कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिग का काम करते थे और बेहद गरीब थे।
यह संयोग है कि इतिहास और संग्राहलय विज्ञान की एक विद्वान लड़की एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सेरामपुर जा पहुंची। इरादा यही था कि यहां मरती हुई कला को इतिहास में दर्ज कर लिया जाए। संग्रहालयों में सजा लिया जाए, पर जब कारीगरों से बात शुरु हुई, तो कमाल हो गया। वहां के हालात देख, 25 वर्षीय युवती स्तब्ध रह गई। अमृतसर में 1944 में जन्मी और दिल्ली न्यूयॉर्क में पढ़ी-लिखी, दुनिया घूम चुकी युवती के मन में सवाल पैदा हो गया कि इस बचे हुए वर्तमान से यह पूछ तो लो, क्या यह इतिहास बनने को तैयार है? वाकई, जितने कारीगर मिले, कोई भी हार मानने को तैयार न था, जहां तक कला निभ जाए, उसकी सेवा हो जाए, इस देश की माटी के कारीगर निभा देना चाहते थे। सेरामपुर ने उस युवती को एक अलग ही संसार में ला खड़ा किया और युवती ने लड़की के एक प्रिंटिंग ब्लॉक को अपनी मुट्ठी में प्यार से सहेजने की कोशिश करते हुए संकल्प लिया कि इस विरल कला को इतिहास में जाने से बचाना होगा।
कारीगरों की गरीबी देखी नहीं जाती थी। एक वस्त्र बनाने में कई-कई दिन लगते थे, तब चंद दिनों का निवाला जुटता था । कारीगरों के पास न अच्छे मकान थे और न अच्छा परिवेश। मैले-कुचैले से माहौल में भी वे राजसी वस्त्र तैयार करने में जुटे थे। उनके बनाए शानदार वस्त्र देख विश्वास नहीं होता था कि इन्हें बनाने वाले दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसते होंगे।
फिर क्या था, उस विद्वान युवती ने वहां सेरामपुर में एक उद्योग की नींव रखी। इसकी शुरुआत कुछ ब्लॉक प्रिंटर और दो मेजों के साथ हुई। कारीगरों को उनके परिवेश से निकालकर कहीं और ले जाना ठीक नहीं था, तो पहले उद्यम के लिए उन्होंने सेरामपुर को ही चुना। कढ़ाईकारों के काम को नए डिजाइन के साथ पेश करने की जरुरत थी। ताकि लोगों को तैयार वस्त्रों में कुछ खास नजर आए और इसके लिए तैयार वस्त्रों में कुछ खास पेश करने की जरुरत थी, उन देशी कारीगरों ने ही सबसे पहले पहचाना कि यह मैडम रितु कुमार हैं, जो कारीगरों के हित में कुछ करना चाहती हैं। रितु ने साड़ियों को डिजाइन करना शुरु किया। कारीगरों ने अपने अंदाज को कुछ बदला और धीरे-धीरे अच्छी साड़ियां उतरने लगीं। कारीगर पूरे मन से बनाने लगे। अब समस्या यह आई कि कोलकाता ही नहीं, देश में कहीं भी ढंग की कोई कपड़े की दुकान न थी। बुटीक कल्चर कल्पना में नहीं था। उस दौर में दिल्ली में रितु कुमार ने अपना पहला बुटीक खोला।
कोलकाता से दिल्ली पहुंचकर साड़ियों बिकने लगीं और उनकी कंपनी चल निकली। मांग बढ़ी, तो शहर-दर-शहर उनके स्टोर खुलने लगे। अनेक प्रकार की लुप्त वस्त्र कलाओं को उन्होंने पेश करना शुरु किया। भारतीय जरदोजी की सदियों पुरानी कला नए डिजाइन के साथ चर्चा में आ गई। ऊंचे दामों में बिकने लगी। कारीगरों की जिंदगी संवरने लगी। कुछ ही वर्षों में रितु कुमार ने अपने वस्त्र शिल्प कारोबार को करोड़ों- अरबों में पहुंचा दिया।
आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ भारतीय डिजाइर के रुप में जानती है। वह देश के उन चुनिंदा सम्मानित उद्यमियों में हैं, जिन्होंने यह साबित किया है कि भारत के पास दुनिया को बेचने के लिए बहुत कुछ है, बस थोड़े नवाचार की जरुरत है।
बेशक, भारतीय वस्त्र शिल्प ने लंबा रास्ता तय किया है, पर उन्हें अब भी संतोष नहीं है। वह अफसोस जताती हैं कि मैं अपने देश के हथकरघे के साथ वह नहीं कर पाई, जो मैने कढ़ाई और प्रिंट के साथ किया। अभी तो देश में बहुत काम शेष है।